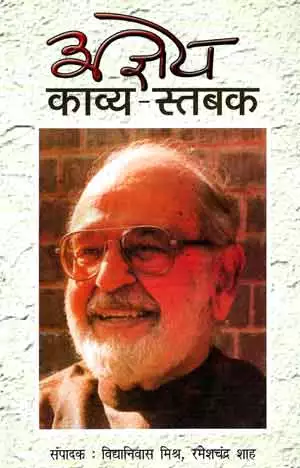|
कविता संग्रह >> अज्ञेय काव्य स्तबक अज्ञेय काव्य स्तबकसच्चिदानंद हीरानन्द वात्स्यायन अज्ञेय
|
184 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है अज्ञेय की 134 कविताओं का संकलन...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
इस स्तबक में 134 कविताएँ संकलित है। प्रत्येक कविता के अंत में रचनाकाल
दिया हुआ है। रचना-प्रकाशन का क्रम भी परिशिष्ट में दे दिया गया है। हमें
यह स्तबक तैयार करते समय अज्ञेय की काव्ययात्रा के साथ होने का जो सुख
मिला, उसके लिए साहित्य अकादमी के हम हृदय से आभारी हैं। हमें विश्वास है
कि यह स्तबक अज्ञेय काव्य के सहृदय पाठकों के रमाने में कृतकार्य होगा।
प्राक्कथन
साहित्य अकादमी के आग्रह पर हम लोगों ने
अज्ञेय की रचनाओं का यह स्तबक
तैयार किया है। इसमें उनकी अप्रकाशित कविताओं में से भी कुछ ली गयी हैं,
जिससे उनकी समूची काव्ययात्रा का पूरा परिदृश्य उपस्थित किया जा सके।
भूमिका के रूप में हम दोनों ने अलग-अलग पक्ष लिये,
‘जीवनयात्रा’ का अंश विद्यानिवास मिश्र ने लिखा,
‘अज्ञेय का कविकर्म’ रमेशचन्द्र शाह ने। कविताओं के
लिए श्रीमती इला कोइराला (वत्सलनिधि की प्रबन्ध न्यासी) से अनुमति मिली
है, उसके लिये हम उनके आभारी हैं।
इस स्तबक में 134 कविताएं संकलित हैं। प्रत्येक कविता के अंत में रचनाकाल दिया हुआ है। रचना-प्रकाशन का क्रम भी परिशिष्ट में दिया गया है। हमें यह स्तबक तैयार करते समय अज्ञेय की काव्ययात्रा के साथ होने का जो सुख मिला, उसके लिए साहित्य अकादेमी के हम हृदय से आभारी हैं। हमें विश्वास है कि यह स्तबक अज्ञेय काव्य के सहृदय पाठकों को रमाने में कृतकार्य होगा।
इस स्तबक में 134 कविताएं संकलित हैं। प्रत्येक कविता के अंत में रचनाकाल दिया हुआ है। रचना-प्रकाशन का क्रम भी परिशिष्ट में दिया गया है। हमें यह स्तबक तैयार करते समय अज्ञेय की काव्ययात्रा के साथ होने का जो सुख मिला, उसके लिए साहित्य अकादेमी के हम हृदय से आभारी हैं। हमें विश्वास है कि यह स्तबक अज्ञेय काव्य के सहृदय पाठकों को रमाने में कृतकार्य होगा।
विद्यानिवास मिश्र
रमेशचन्द्र शाह
रमेशचन्द्र शाह
अज्ञेय की जीवन यात्रा
अज्ञेय की कविताओं का संकलन समग्रतर बनाने के
लिये मैं पिछले पन्द्रह
वर्षों से सोच रहा हूँ। प्रारम्भ में दी हुई जीवनी को फिर से लिखना चाहता
हूँ-केवल कुछ जोड़-घटाकर नहीं, आमूल ढाँचे को बदलकर लिखना चाहता था, वह कई
कारणों से नहीं हो सका। सबसे बड़ा कारण यह रहा कि मैं कृति अज्ञेय को पूरी
तरह समझना चाहता था और वह समझना आसान नहीं था। डूबता ही रहा, तिरकर किसी
किनारे लग नहीं सका। मैं उसके स्नेह के प्रकाश के घेरे में ऐसा घिरता गया
कि उनके कृतित्व का उसके व्यक्तित्व का संयोजन न कर सका। आज वह स्नेह
देनेवाला व्यक्ति नहीं है, उसके स्नेह की अहर्निश जीती-जागती स्मृति है और
यह स्मृति ही लिखने में बाधक है। उन्नीस सौ सत्तासी में, सत्ताईस मार्च को
यह भीतरी जानकारी लूँ और तब उनकी जीवनी लिखूँ। पहले भी उनके साथ बर्कले
में दिन में सात-सात घण्टे बात करके (क्योंकि उस समय विश्वविद्यालय बंद
था, और कोई दूसरा कार्य न भाई के पास था, न मेरे) मैंने मौन गम्भीरता की
राख कुरेद-कुरेद कर वह आग खोदी थी, जो अज्ञेय की वैश्वानरी खोज थी। मैंने
उस आग के आलोक में फिर से उनकी कविताएँ पढ़ी और ‘आज के लोकप्रिय
हिन्दी कवि : अज्ञेय’ का पहला संस्करण बर्कले में ही तैयार
किया। पहला संस्करण, जहाँ तक मुझे याद है, अप्रैल उन्नीस सौ तिरसठ में छपा
था। उसके बाद अनेक संस्करण हुए थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहे पर 1986 से
मैं इस संग्रह को सर्वथा नया रूप देना चाहता रहा हूँ और कहीं-न-कहीं अटक
जाता रहा हूँ। कहीं आत्मीयता जितनी बढ़ती है, उतनी ही दूरी भी बढ़ती है,
यह असमंजस ही कारण हो या अज्ञेय के विचारक पक्ष के रखने पर उनकी कविताओं
में आयी हुई सादगी एकदम अनपहचानी लगी, यह कारण हो-संकल्पित कार्य नहीं हो
नहीं सका। वह संकल्प 86-87 में फिर जगा और स्वर्गीय भाई से जो वादा किया
था कि जून 87 में भीमताल के पास वाले, नये खरीदे मकान में पन्द्रह दिन साथ
बितायेंगे और यहाँ किताब पूरी करेंगे, यह वादा कराने वाला स्वयं धोखा दे
गया (यद्यपि कहा यह था ‘‘देखिये इस बार
‘डिच’ न कीजियेगा’’-हम लोगों के
बीच कई एक यात्राओं में साथ-साथ रहने की योजनाएँ आँख-मिचौनी का खेल-खेल
चुकी थीं) इसका आधार भी बहुत ज़बर्दस्त था और तीन वर्ष बीत गये, मैं अपना
संकल्प पूरा न कर सका, क्योंकि इस अवधि में इस तथ्य से समझौता नहीं कर सका
कि वे नहीं रहे। वे छोड़कर चले जा सकते है। आवेग अभी गया नहीं, पर अब लगा
कि संगह की भूमिका को नये सिरे से लिखूँ ही और उन्हीं के साथ बैठकर छाँटी
गयी कविताओं का नये सिरे से अनुक्रम लगाऊँ और उनकी जीवनी पूरी
करूँ-निर्णायक बन कर नहीं, उनके क्रांतियुगोत्तर साहित्यिक जीवन का
सहयात्री बनकर। मैं एक विचित्र किस्म का सहयात्री था-शिष्य या भक्त बनकर
उनके पीछे नहीं लगा; हमजोली, मित्र, साथी के रूप में कोई छूट नहीं ली,
तटस्थ जीवनी लेखक की तरह प्रतिक्षण का लेखा-जोखा नहीं लेता रहा। उनसे दूर,
पर उनके स्नेह के कारण उनके नज़दीक, उनकी सहज कृपा के कारण उनके बहुत समीप
रहा, उनसे अधिक कुछ पूछे बिना अनेक उत्तर पाता रहा। उनके सान्निध्य में एक
जादू था जो, समुद्दीपित होता रहा। इस समुद्दीपन (रेडिएशन) का अनुभव जो
उनके पास गया है, उसने अवश्य किया है। कभी-कभी विश्वास नहीं होता कि उनके
स्नेह कि पात्रता मुझसे है कि नहीं और वह अविश्वास उनके एकाक्षर-सम्बोधन,
आशीष, अभिवादन जो भी समझें ‘जय’ में विलुप्त हो जाता
था। मिलने पर ‘जय’ और विदा होते हुए
‘जय’। प्रत्येक स्थिति में प्रतीक्षा, उत्सुक
प्रतीक्षा का भाव मन से छूट नहीं सकता था और यह न छूटना ही प्रेरित करता
है कि एक-दूसरे से गुँथे हुए अनन्त स्मृतियों के सूत्रों को सुलझा नहीं
पाऊँ, तब भी उन्हें एक सूत के रूप में बट तो दूँ ही।
अज्ञेय के जीवन का अंतिम सप्ताह अद्भुत विषाद, अद्भुत वैराग्य और अद्भुत उछाह से भरा रहा। भोपाल जाने के पूर्व यह इच्छा व्यक्त की कि अब मैं अपने को खींचकर कुछ अपने भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। भोपाल में कविता के उत्सव के केन्द्र में रहकर कविता के लिये उत्सुकता जगाते रहे और इसी बीच हलका संकेत भी देते रहे कि यह सब दीये की लौ की अंतिम भभक है। दिल्ली आकर एक रात पंडित जसराज के संगीत में डूबे। दूसरे दिन उन्हें घर बुलाया और कलाकार के साथ बात करते-करते कुछ अस्तित्व जैसा अनुभव किया और आराम करने चले गये। अंतिम दिन तक, बल्कि अंतिम रात तक सजग कला साहित्य संस्कृति के प्रतिभू बने रहकर अपनी साँसें उन्होंने बटोरीं और भारतीय साहित्य के सम्पूर्ण शरीर हमारी आँखों से 4 अप्रैल 1987 को विदा ले गये। 75 वर्ष उसके पहले साल पूरे हो चुके थे और उसके अनेक उत्सव यहाँ-वहाँ बड़ी सुरुचि से मनाये जा चुके थे। कुछ विचार था मानव मूल्यों को केन्द्र में रखकर, एक स्तरीय निबन्ध संग्रह उनके सम्मान में छपाया जाये और उनकी जीवन-साधना को इसके द्वारा रूपायित किया जाये, क्योंकि वह जो कुछ थे, मानव मूल्यों को पूरी तरह अर्पित व्यक्ति थे। धीर, उदात्त और दुर्धर्ष योद्धा थे, निर्भीक पर दुःसाहसी नहीं, सत्यान्वेषी पर अकरुण नहीं, विचारक पर शब्दजाली नहीं, दिग्विजयी पर अंहकारी नहीं, गहरे आस्तिक, पर विश्वास के डिंडिभवादक नहीं, समाहित पर आत्मलीन नहीं, स्रष्टा से अधिक पाठक-और पाठक से अधिक आस्वादन और सम्प्रेषण के मर्मज्ञ-पर सम्प्रेषण के लिये उतावले नहीं, अतिशय संवेदनशील पर संयत कवि विचारक अज्ञेय के जीवन की भूमिका की इतनी भूमिका के बाद उनकी जीवन-यात्रा के विवरण पर आता हूँ।
अज्ञेय की जीवन-यात्रा और काव्य-यात्रा आधुनिक हिन्दी कविता और आधुनिक भारत के भीतर के आवेगों और असंयत-संयत दोनों प्रकार के उबालों; सम्ष्टि से व्यष्टि और व्यष्टि से समष्टि के उदय; स्वप्न-भंग और स्वप्न-भंग से जन्मे विषाद के सर्वस्वीकारी और सर्वसमर्पित भाव में परिणमन; अपनी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान; अपनी जातीय लय की खोज; पश्चिमी शिक्षा के संस्कार को स्वीकार करते हुए भी अपनी जातीय स्वायत्तता, अपने अखण्ड भारतीय व्यक्तित्व को पाने के लिये अनेक मार्गो के अनुसंधान (कुछ भटकने के, कुछ सही दिशा में जाने के कुछ खोने के, कुछ पाने के अंततः कुछ से कुछ और होने के लिये ये मार्ग तलाशे गये और एक के बाद एक त्यागे गये पर ये सभी मार्ग कहीं-न-कहीं हमारे व्यक्तित्व के अंग बने) का समवर्ती इतिहास है। अज्ञेय जन्म से लेकर वृद्ध तक यात्री रहे-घुम्मकड़ यात्री नहीं, न कोरे सैलानी यात्री : देश या विदेश में उन्होंने प्रकृति के मनोरम स्थलों की यात्रा इस भाव से की, जैसे प्रत्येक स्थल आनन्दमयी चैतन्य सत्ता का साकार विग्रह है। वे देश-विदेश की तरह-तरह की मानव भंगिमाओं में कहीं कुछ गहरे सत्य का आलोक पाते थे पर यायावर होते हुए भी घर के बिना और घर वापसी की आशा के बिना नहीं। वे कहते थे, ‘‘घर रहने के लिये उतना नहीं होता, जितना कि वापस जाने के लिये होता है।’’ वे इतने विजातीय साहित्यों संस्कृतियों में रमे हुए थे, फिर भी वे भारत के घर से निरंतर बँधे रहे। जाने के पहले बड़े चाव से और उछाह से एक ही काम किया-घर के पास के नीम की डालियों के बीच काठ का घर बनाया और उस तक पहुँचने के लिये काठ की सीढ़ियाँ बनायीं। यह घर बच्चों के और चिड़ियों के खेलने के लिये बनाया गया था। शायद अज्ञेय के कवि के भीतर भी एक बच्चा था। एक ऊर्ध्वंग आकांक्षा लिये एक हारिल पंछी था, जो आकाश में खोना चाहता था और हाथ में अपनी प्रिय धरती का तिनका लिये था। 1938 में जेल की लम्बी यात्रा से लौटने के बाद अज्ञेय ने अपने हारिल को पुकारा था:-
अज्ञेय के जीवन का अंतिम सप्ताह अद्भुत विषाद, अद्भुत वैराग्य और अद्भुत उछाह से भरा रहा। भोपाल जाने के पूर्व यह इच्छा व्यक्त की कि अब मैं अपने को खींचकर कुछ अपने भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। भोपाल में कविता के उत्सव के केन्द्र में रहकर कविता के लिये उत्सुकता जगाते रहे और इसी बीच हलका संकेत भी देते रहे कि यह सब दीये की लौ की अंतिम भभक है। दिल्ली आकर एक रात पंडित जसराज के संगीत में डूबे। दूसरे दिन उन्हें घर बुलाया और कलाकार के साथ बात करते-करते कुछ अस्तित्व जैसा अनुभव किया और आराम करने चले गये। अंतिम दिन तक, बल्कि अंतिम रात तक सजग कला साहित्य संस्कृति के प्रतिभू बने रहकर अपनी साँसें उन्होंने बटोरीं और भारतीय साहित्य के सम्पूर्ण शरीर हमारी आँखों से 4 अप्रैल 1987 को विदा ले गये। 75 वर्ष उसके पहले साल पूरे हो चुके थे और उसके अनेक उत्सव यहाँ-वहाँ बड़ी सुरुचि से मनाये जा चुके थे। कुछ विचार था मानव मूल्यों को केन्द्र में रखकर, एक स्तरीय निबन्ध संग्रह उनके सम्मान में छपाया जाये और उनकी जीवन-साधना को इसके द्वारा रूपायित किया जाये, क्योंकि वह जो कुछ थे, मानव मूल्यों को पूरी तरह अर्पित व्यक्ति थे। धीर, उदात्त और दुर्धर्ष योद्धा थे, निर्भीक पर दुःसाहसी नहीं, सत्यान्वेषी पर अकरुण नहीं, विचारक पर शब्दजाली नहीं, दिग्विजयी पर अंहकारी नहीं, गहरे आस्तिक, पर विश्वास के डिंडिभवादक नहीं, समाहित पर आत्मलीन नहीं, स्रष्टा से अधिक पाठक-और पाठक से अधिक आस्वादन और सम्प्रेषण के मर्मज्ञ-पर सम्प्रेषण के लिये उतावले नहीं, अतिशय संवेदनशील पर संयत कवि विचारक अज्ञेय के जीवन की भूमिका की इतनी भूमिका के बाद उनकी जीवन-यात्रा के विवरण पर आता हूँ।
अज्ञेय की जीवन-यात्रा और काव्य-यात्रा आधुनिक हिन्दी कविता और आधुनिक भारत के भीतर के आवेगों और असंयत-संयत दोनों प्रकार के उबालों; सम्ष्टि से व्यष्टि और व्यष्टि से समष्टि के उदय; स्वप्न-भंग और स्वप्न-भंग से जन्मे विषाद के सर्वस्वीकारी और सर्वसमर्पित भाव में परिणमन; अपनी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान; अपनी जातीय लय की खोज; पश्चिमी शिक्षा के संस्कार को स्वीकार करते हुए भी अपनी जातीय स्वायत्तता, अपने अखण्ड भारतीय व्यक्तित्व को पाने के लिये अनेक मार्गो के अनुसंधान (कुछ भटकने के, कुछ सही दिशा में जाने के कुछ खोने के, कुछ पाने के अंततः कुछ से कुछ और होने के लिये ये मार्ग तलाशे गये और एक के बाद एक त्यागे गये पर ये सभी मार्ग कहीं-न-कहीं हमारे व्यक्तित्व के अंग बने) का समवर्ती इतिहास है। अज्ञेय जन्म से लेकर वृद्ध तक यात्री रहे-घुम्मकड़ यात्री नहीं, न कोरे सैलानी यात्री : देश या विदेश में उन्होंने प्रकृति के मनोरम स्थलों की यात्रा इस भाव से की, जैसे प्रत्येक स्थल आनन्दमयी चैतन्य सत्ता का साकार विग्रह है। वे देश-विदेश की तरह-तरह की मानव भंगिमाओं में कहीं कुछ गहरे सत्य का आलोक पाते थे पर यायावर होते हुए भी घर के बिना और घर वापसी की आशा के बिना नहीं। वे कहते थे, ‘‘घर रहने के लिये उतना नहीं होता, जितना कि वापस जाने के लिये होता है।’’ वे इतने विजातीय साहित्यों संस्कृतियों में रमे हुए थे, फिर भी वे भारत के घर से निरंतर बँधे रहे। जाने के पहले बड़े चाव से और उछाह से एक ही काम किया-घर के पास के नीम की डालियों के बीच काठ का घर बनाया और उस तक पहुँचने के लिये काठ की सीढ़ियाँ बनायीं। यह घर बच्चों के और चिड़ियों के खेलने के लिये बनाया गया था। शायद अज्ञेय के कवि के भीतर भी एक बच्चा था। एक ऊर्ध्वंग आकांक्षा लिये एक हारिल पंछी था, जो आकाश में खोना चाहता था और हाथ में अपनी प्रिय धरती का तिनका लिये था। 1938 में जेल की लम्बी यात्रा से लौटने के बाद अज्ञेय ने अपने हारिल को पुकारा था:-
उड़ चल, हारिल, लिये हाथ में यही अकेला ओछा
तिनका,
ऊषा जाग उठी प्राची में-कैसी बाट भरोसा किनका।
शक्ति रहे तेरे हाथों में-छुट न जाय यह सृजन की,
शक्ति रहे तेरे हाथों में-रुक न जाये यह गति जीवन की।
ऊपर-ऊपर-ऊपर-ऊपर-बढ़ा चीरता चल दिङ् मंडल,
अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल।
मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है ?
तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है ?
आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा
दृढ़ ध्वज-दंड बना यह तिनका सूने पथ का एक सहारा।
ऊषा जाग उठी प्राची में-कैसी बाट भरोसा किनका।
शक्ति रहे तेरे हाथों में-छुट न जाय यह सृजन की,
शक्ति रहे तेरे हाथों में-रुक न जाये यह गति जीवन की।
ऊपर-ऊपर-ऊपर-ऊपर-बढ़ा चीरता चल दिङ् मंडल,
अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल।
मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है ?
तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है ?
आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा
दृढ़ ध्वज-दंड बना यह तिनका सूने पथ का एक सहारा।
अज्ञेय के उस हारिल ने अनन्त की पावन धूलि
बनकर अनन्त की अमरता छू ली, सही
है, पर घर उसको घेरे रहा। कोई एक ठिकाने के रूप में नहीं बल्कि, आत्मीयता
के आश्वासन के रूप में। प्रकाश के घेरे के भीतर घर की चाह और बेघर होने का
भाव दोनों ताना-बाना बुनकर उनको रचते रहे। संयोग से उनकी मानव नियति यही
थी-जन्म हुआ कुशीनगर के एक खुदाई शिविर में, किसी छोलदारी के नीचे-उस
स्थान की बड़ी मुश्किल से पहचान बड़ी बहिन जी ने करायी। बचपन अपने पिता के
साथ बीता पुरातत्व केन्द्रों में। पढ़ाई स्कूल में लगभग नहीं ही हुई,
क्योंकि ऊदकमण्डलम् (ऊटी) में भर्ती होते ही एक अंग्रेजी बच्चे ने गाली दी
और उसकी ठुकाई करके स्कूल का मुँह नहीं देखा। दक्षिण भारत में रम्य
नीलगिरी की छाया में पिता के कड़े अनुशासन और बड़ी बहन के मातृ-कल्प
वात्सल्य की छाया में बचपन बीता। घर पर ही पढ़ाई कर पंजाब की मैट्रिकुलेशन
परीक्षा दी। सीधे मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में इन्टरमीडिएट में भर्ती
हुए और इंटरमीडिएट कर लाहौर के फोरमैन कॉलेज में बी.एस.सी. में प्रवेश
लिया और वहीं से क्रांतिकारी का मार्ग अपनाया और फिर वहाँ से हिमालय की
पहाड़ियों तक न जाने कहाँ लुकते-छिपते एक दिन गिरफ़्तार हुए और जेल के
सींखचों में बन्द हो गये और राजद्रोहकी सजा फाँसी आँखों के सामने झूलती
रही। प्रक्रिया की त्रुटि के कारण छूटे, फिर लाहौर गये, जेल में नज़रबंद
हुए और उसके बाद किसान आंदोलन, पत्रकारिता, सेना की नौकरी, साहसिक एकाकी
यात्राओं का सिलसिला सही मानों में भारत की खोज और दिल्ली, मेरठ, आगरा,
कलकत्ता, पूर्वी भारत, इलाहाबाद, दिल्ली फिर इलाहाबाद फिर दिल्ली में मकान
पर मकान बदलते हुए, काम पर काम छोड़ते हुए उन्नीस सौ सत्तावन से विदेश
यात्राओं का क्रम-उपक्रम उन्नीस सौ छियासी तक चलता रहा। ये यात्राएँ जितनी
बाहर थीं उतनी ही भीतर भी। जितना खोना थीं, उतना ही पाना थी। जितनी
आत्मीयता की तलाश थी, उतनी ही बाहर कर दिये जाने की कसक थी। ऐसे अविश्रांत
यात्री को इतना निश्चिंत और अनुद्विग्न देखते ही लोग अचरज में पड़ जाते
थे, कभी-कभी परेशान भी हो जाते थे कि कौन-सा जादू है कि इतनी उथल-पुथल में
रहने वाला आदमी अपने को इतना शांत और समाहित बना लेता है; पर ढोंग की छाया
भी अज्ञेय को छू नहीं गयी थी। वे जो कुछ थे, उसमें बनवा नहीं था। सब कुछ
सहज भाव से आता था। अच्छे भोजन का स्वाद, ज़रूरी नहीं कि वह अमीरी का भोजन
हो, अच्छे कपड़े और उसकी अच्छी सिलावट की पहचान, ज़रूरी नहीं कि वो कपड़े
महँगे हो, घर के विन्यास का कौशल कि प्रवेश करते ही पता चल जाये कि किसी
खास आदमी के घर आये हैं-कहीं सामान की भीड़ नहीं, कहीं प्रदर्शन,
तड़क-भड़क नहीं। हर चीज़ का हर चीज़ से ऐसा मेल कि लगे कि उनके बीच का
जाने कब का रिश्ता है। अपने हाथ से लगाये फूल-पत्तियों से उतना ही प्यार,
जितना अपने आप उगे पौधों-औषधियों और पेड़ों से प्यार, अन्याय न सह सकने का
आक्रोश और अपनी भावनाओं को संयत रखने का अपार धैर्य, वाणी की कुशलता और
मौन का अभ्यास, यह सभी देखने में एक-दूसरे के विपरीत लगते हैं, पर वस्तुतः
एक दूसरे के पूरक हैं और पूरक नहीं तो समग्र व्यक्तित्व बनेगा ही नहीं और
अज्ञेय का व्यक्तित्व समग्र है। फाँसी के तख्ते से उतर कर आया व्यक्ति एक
बार मृत्यु के द्वार को देख लेता है तो उसका जीवन मरणधर्मा नहीं रह जाता
है, वह अमर हो जाता है।
1986 में उनका अमृत महोत्सव मनाया गया-जो अमृत महोत्सव मनाया गया, वह बहुत ही सार्थक था। उसकी स्मृतियों में एक स्मृति मेरे मन पर गहरी छाप छोड़े हुए है। कुमार गंधर्व ने मीरां और कबीर के पदों का गायन किया था, उसमें एक पद के बोल थे ‘‘हम सब में, सब हम में, हम फिर बहुरि अकेला।’’ मुझे आज लगता है कि वह पद उनमें समा गया है, उनका वह भरा हुआ अकेलापन कहीं दूर ध्रुव तारे की तरह दिग्बोध कराता है और कहता है राह तुम्हारी हो, तुम्हारी बनायी हो, दिशाएँ बंधन नहीं है-दिशाएँ मुक्त हैं, ठहराव से। ऐसे व्यक्ति की जीवनी किस अनुक्रम में बाँधे समझ में नहीं आता। वहाँ से शुरू करें, जहाँ से मैं उन्हें जानता हूँ या वहाँ से शुरू करें, जिसके बारे में उनसे जाना है। बहुत कुछ उनकी भी स्मृति में नहीं है-मुझसे पन्द्रह वर्ष का यह अन्तर उन्होंने रखा ही नहीं और यह भ्रम ही पैदा किया कि हम आगे पीछे ही जन्मे हुए हैं। जब से उन्हें जाना, तब से उन्हें भाई ही कहा, भाई ही मानता रहा और वे भी भाई ही कहते रहे, केवल जब परिहास या उलाहने की मुद्रा में आते तो ‘पंडितजी’ कहते, ऐसे भाई की कहानी कहूँ या फिर अन्त से शुरू करें, जैसे कि महाभारत, श्रीमद्भागवत् जैसे काव्य-इतिहासों में हुआ है ? नहीं, मुझे जीवनी देनी है, एकदम सपाट नहीं, पर जीवनी क्रमबद्ध होती है, क्रमबद्ध ही जीवनी देने की कोशिश करूँगा।
उनका जन्म वत्स गोत्र के भणोत सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पितामह पंडित मूलचन्द शास्त्री ज्योतिषी थे-संस्कृत विद्या, कुलागत विद्या थी, उनका मूल अभिजन्म जालंधर जिले के कर्तापुर गाँव में। उनके पिता डॉ. हीरानन्द शास्त्री भारतीय पुरातत्व विभाग की सेवा में उच्च अधिकारी थे। वे संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित थे और प्राचीन लिपियों में ऐसे मर्मज्ञ थे, जैसे वे लिपियाँ उन्हें मिट्टी में मिली हों। उन्हें उन महत्त्वपूर्ण खुदाइयों का श्रेय प्राप्त है, जिन्होंने भारतीय इतिहास समझने के लिये सबसे स्पष्ट प्रमाण दिये हैं। कुशीनगर में भगवान् बुद्ध के महा-परिनिर्वाण स्थल को इन्होंने खोद निकाला है। नालन्दा की खुदाई ने भारतीय शिक्षा के केन्द्रों का आकार खड़ा किया। काशी में राजघाट की खुदाई ने कला-वैभव की रत्न-राशि दी। यद्यपि वे मोहन-जोदड़ों और हड़प्पा की संस्कृतियों के उद्घाटक थे, अंग्रेज साम्राज्य में यह श्रेय उनके अंग्रेज प्रभुओं को मिला। माँ दयावती देवी की चौथी संतान थे। सबसे सत्यवती जी, उनके बाद ब्रह्मानंद जी, उसके बाद जीवानन्द जी, जो 1934 में ही चल बसे; और उनसे छोटे वत्सराज जो बड़ौदा विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर वहीं रहते हैं। उसके बाद नित्यानन्द जी जो कि बिहार में क्रांतिकारी के रूप में कार्य करते रहे, वहीं बस गये हैं और उनसे छोटे पूर्णानंद जी जो काफ़ी कम उम्र में ही चले गये। उसके बाद रामानन्द जी और सबसे छोटी आनन्द लता जी, जिन्हें वे अन्ना जी कहकर बुलाते थे।
जन्म फल्गुन शुक्ल सप्तमी संवत् 1967 तदनुसार 7 मार्च, 1911 को कसया पुरतत्त्व-खुदाई शिविर में। बचपन 1911 से 15 तक लखनऊ में। शिक्षा का प्रारम्भ संस्कृत-मौखिक परम्परा से हुआ। 1915-19 तक श्रीनगर और जम्मू में। यहीं पर संस्कृत पंडित से रघुवंश, रामायण, हितोपदेश, फ़ारसी मौलवी से शेख़ सादी और अमेरिकी पादरी से अंग्रेज़ी की शिक्षा घर पर शुरू हुई। शास्त्रीजी को स्कूली शिक्षा में विश्वास नहीं था। बचपन में व्याकरण के पंडित से मेल नहीं हुआ। घर पर धार्मिक अनुष्ठान स्मार्त ढंग के होते थे। बड़ी बहन, जो लगभग आठ वर्ष बड़ी थी, जितना अधिक स्नेह करती थी, उतने ही दोनों बड़े भाई (ब्रह्मानन्द, जीवानन्द, जो 34 में दिवंगत हो गये) प्रतिस्पर्द्धा रखते थे। छोटे भाई वत्सराज के प्रति सच्चिदानन्द का स्नेह बचपन से ही था। 1919 में पिता के साथ नालन्दा आये, इसके बाद 1925 तक पिता के ही साथ रहे। पिताजी ने ही हिन्दी लिखाना शुरु किया। वे सहज और संस्कारी भाषा के पक्ष में थे। हिन्दुस्तानी के सख्त ख़िलाफ़ थे। नालन्दा से शास्त्रीजी पटना आये और वहीं स्व. काशीप्रसाद जायसवाल और स्व. राखालदास वन्द्योपाध्याय से इस परिवार का सम्बन्ध हुआ, पटना में ही अंग्रेज़ी से विद्रोह का बीज सच्चिदानंद के मन में अंकुरित हुआ। शास्त्रीजी के पुराने मित्र रायबदाहुर हीरालाल ही उनकी हिन्दी भाषा की लिखाई की जाँच करते। राखालदास के सम्पर्क में आने से बाड्ल़ा सीखी और इसी अवधि में इण्डियन प्रेस से छपी बाल रामायण, बाल महाभारत, बालभोज, इंदिरा (बंकिमचन्द्र) जैसी पुस्तकें पढ़ने को मिली और हरिनारायण आप्टे और राखालदास बन्द्योपाध्याय के ऐतिहासिक उपन्यास इसी अवधि में पढ़े गये। 1921-24 तक ऊटकमंड में रहे। यहाँ नीलगिरि की श्यामल उपत्यका ने बहुत अधिक प्रभाव डाला। 1921 में उडिपी के मध्वाचार्य के द्वारा इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसी मठ के पंडित ने छह महीने तक संस्कृत और तमिल की शिक्षा दी। इसी समय ‘भणोत’ से ‘वात्स्यायन’ में परिवर्तन भी हुआ, जो प्राचीनतम संस्कार को नये उत्साह से जीने का एक संकल्प था। पिता ने संकीर्ण प्रादेशिकता से ऊपर उठकर गोत्रनाम का प्रचलन कराया। इसी समय पहली बार गीता पढ़ी। पिताजी के आग्रह से अन्य धर्मों के ग्रन्थ भी पढ़े और घर पर ही पिताजी के पुस्तकालय का सदुपयोग शुरू किया। वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, लांगफेलो और व्हिटमैन की कविताएँ इस अवधि में पढ़ीं। शेक्सपियर, मारलो, वेब्स्टर के नाटक तथा लिटन, जार्ज एलियट, थैकरे, गोल्डस्मिथ, तोल्सतोय, तुर्गनेव, गोगोल, विक्टर ह्यूगो तथा मेलविल के उपन्यास भी पढ़े गये। लयबद्ध भाषा के कारण टेनिसन प्रभाव बड़ा गहरा पड़ा। टेनिसन के अनुकरण में, अंग्रेजी में ढेरों कविताएँ भी लिखीं।
उपन्यासकारों में ह्यूगों का प्रभाव, विशेष कर उनकी रचना ‘टॉयलर्स ऑफ दी सी’ का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इसी अवधि में विश्वेश्वर नाथ रेऊ तथा गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा की हिन्दी में लिखी इतिहास की रचनाएँ पढ़ने को मिलीं तथा मीरा, तुलसी के साहित्य का अध्ययन भी इन्होंने किया। साहित्यिक कृतित्व के नाम पर इस अवधि की देन है ‘आनन्द-बन्धु’ जो इस परिवार की निजी पत्रिका थी। इस पत्रिका के समीक्षक थे हीरालालजी और डाक्टर मोद्गिल। इसी अवधि में एक छोटा उपन्यास भी लिखा और इसी अवधि में जब मौट्रिक की तैयारी ये कर रहे थे, माँ के साथ इन्होंने जलियाँवाला बाग़ काण्ड की घटना के आसपास पंजाब की यात्रा की थी और अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह की भावना ने जन्म लिया था। एक घटना भी ब्लैकस्टोन नामक अंग्रेज़ अधिकारी के साथ घट चुकी थी। वह शास्त्रजी औऱ राखालदास के साथ यात्रा कर रहा था। डिब्बे में राखालदास की पत्नी भी थी। वह स्नानकक्ष से अर्द्धनग्न डिब्बे के भीतर आया। शास्त्रीजी ने उससे पूछा, ‘‘क्या इस रूप में तुम किसी अंग्रेज़ महिला के सामने आ सकते थे ?’’ उत्तर में वह कुछ बोला नहीं, हँसता रहा। शास्त्रीजी ने उसे ठठाकर डिब्बे से बाहर फेंक दिया। उसने आजीवन शत्रुता निभायी, यहाँ तक कि पिता द्वारा किये गये इस अपमान का बदला पुत्र से चुकाया, जब वे लाहौर क़िले में नज़रबन्द हुए।
दूसरी घटना का जिक्र वात्स्यायन ने संवत्सर में किया है। इनके पिताजी ने अपनी किसी पुरातत्व यात्रा में एक जगह देखी थी, जहाँ दो बूढ़े सिपाही तोप के गोले बनाते और किसी ढूह पर निशाना लगाते। एक तरह से उनके ऊपर इसका पागलपन छा गया था। ये दोनों बूढ़े सिपाही 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के बचे सिपाही थे। जो अंग्रेज़ों से प्रतिशोध लेने का यही उपाय निकाल सके थे और काल बीत गया था, परिस्थितियाँ बीत गयी थीं पर ये दोनों बूढ़े बीते काल के ऐसे संसक्त थे कि इनके लिये दूसरी वास्तविकता रह नहीं गयी थी। इस दृश्य का पंडित हीरानन्द शास्त्री पर गहरा प्रभाव पड़ा था और उस पागलपन में भी उन्हें एक दुर्धर्ष संकल्प दिखायी पड़ा था। शास्त्री जी सरकारी चाकरी में तो थे, पर अपने देश के लिये अभिमान और देश के लिए स्वाधीनता का स्वपन दोनों ही उनके कर्म और उनके हिन्दी लेखन में उद्भासित थे। उन्होंने एक तरह से ऐसे लोगों का एक समुदाय ही बनाया था, जो कला-चिन्तन और इतिहास-चिन्तन में स्वदेशी हों। इस समुदाय में थे स्वर्गीय राखालदास बन्द्योपाध्याय, जिन्हें लोग आर्डी बनर्जी के नाम से अधिक जानते हैं, स्वर्गीय विश्वेश्वरनाथ रेऊ, गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी। इन सबका गहरा प्रभाव भाई पर पड़ा और उनका स्वदेशीपन इस धूप-छाँह में परिपक्व हुआ। इनके पिताजी कठोर थे, बड़े व्यवस्था-प्रिय भी थे पर अपने लड़कों में भाई को कुछ अधिक मानते थे, शायद अपना विफल मनोरथ उनमें चरितार्थ होना देखना चाहते थे, इसीलिये मैंने धूप-छाँह की उपमा दी।
तीसरी घटना ऊटी में स्वयं सच्चिदानन्द के साथ घटी थी, जब वे दो-तीन महीने अंग्रेज़ों के साथ स्कूल में पढ़ने गये। वहाँ अंग्रेज़ी लड़कों की मरम्मत कर के स्कूल में इन्हें कार्ड मिला, जिसे फेंककर ये घर चले आये। 1925 में पंजाब से मैट्रिक की प्राइवेट परीक्षा दी और उसी वर्ष इण्टरमीडिएट साइंस पढ़ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। यहाँ उन्होंने गणित, भौतिकशास्त्र और संस्कृत विषय लिये थे। यहाँ इनके अंग्रेज़ी के प्रोफ़ेसर हेण्डरसन ने (जिन्हें त्रिशंकु समर्पित की गयी) साहित्य के अध्ययन की प्रेरणा दी। ये स्वयं भारत की भक्त थे। इन्हीं के साथ रवीन्द्रनाथ ने अध्ययन की स्थापना की और रस्किन के सौन्दर्यशास्त्र तथा आचारशास्त्र का अध्ययन किया। कला-क्षेत्रों के बीच में घूमते-घूमते स्थापत्य और शिल्प दोनों का राग-बोध परिपक्व होता गया। दक्षिण के मन्दिर और नीलगिरि के दृश्य ने उन के व्यक्तित्व में प्रकृति-प्रेम और कला-प्रेम को निखार दिया। मद्रास में सामाजिक विषमता की चेतना जगने लगी थी और मन में जाति के विरुद्ध विद्रोह इसी अवधि में उमड़ना शुरू हुआ। शास्त्रीजी स्वयं जाति में विश्वास न करके वर्ण में विश्वास करते थे और पुत्रों से आशा करते थे कि ब्राह्मण वर्ण का स्वभाव-त्याग, अभय और सत्य-उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
बचपन से किशोरावस्था तक की यह अवधि उलझन और आकुलता के बीच कठिन अध्यवसाय की अवधि है। एक ओर परिवार के और बाहर के अनेक प्रकार के प्रिय-अप्रिय प्रभावों ने उन के चित्त को उद्वेलित किया, तो दूसरी ओर पिता के कठिन अनुशासन ने परिश्रम में लगातार लगाये रखकर मन और शरीर को संयम में ढाला। बचपन में इन्हें ‘सच्चा’ के नाम से पुकारा जाता था और जब-जब इन की सच्चाई पर विश्वास नहीं किया गया, इन्होंने मौन विद्रोह किया।
बड़ी बहन जी ने बताया था कि एक बार पिताजी की कोई चीज़ मिल नहीं रही थी। भाई को मालूम था कि किसने ली थी। पिताजी ने एक-एक कर सबसे पूछे-तुमने ली है ? सबने पिटाई के डर से इन्कार कर दिया। भाई ने भी इन्कार किया और सबका क्रोध इन पर उतरा। पिटाई के बीच में भी चिल्लाते रहे कि मैं जानता हूँ किसने ली है, पर मैं बताऊँगा नहीं। बड़ी बहन रक्षा में खड़ी हो गयी-सच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, न कभी किसी की शिकायत करेगा। वे विनोद से कहती थी कि वह हमेशा से बड़ा ज़िद्दी रहा है, जो ठान ले, करके रहेगा।
एक बार की घटना ऐसी है कि बड़े भाई में और इसमें होड़ लगी कि चौदह रोटी कौन खा सकता है। बड़े भाई ने कहा कि तुम खोओ तो तुम्हें मैं इनाम दूँगा। ये खाने बैठे, पिताजी को इसकी सूचना मिली, उन्होंने बड़े भाई को डाँटा और इनसे कहा कि तुम अब न खाओ, उठ जाओ। ये चौदह के आसपास तक पहुँच रहे थे, अपने मन से उठे नहीं इसलिए इन्होंने भाई से इनाम माँगा। उन्होंने देने से इनकार कर दिया तो मौन विरोध में इसलिए खाना ही कम कर दिया। इस प्रकार की आत्म-पीड़क क्रोध इनमें बहुत दिनों तक रहा हौ और इसी क्रोध में आकर इन्होंने अपनी आर्थिक बर्बादी भी कम नहीं की है।
1927 में लाहौर के फोरमैन कॉलेज में ये बी.एस.सी में भर्ती हुए। इसी कॉलेज में नवजवान भारत सभा के सम्पर्क में आये और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख सदस्य आज़ाद, सुखदेव और भगवतीचरण बोहरा से परिचय हुआ। इस कॉलेज में बी.एस.सी. तक तो ये सक्रिय रूप से क्रान्तिकारी आन्दोलन में प्रविष्ट नहीं हुए थे, यद्यपि 1921 में पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ, उसमें ये स्वयंसेवक अफ़सर के रूप में मौजूद थे। यहीं इन्हीं के स्वयंसेवक दल ने उन लोगों को ज़बरदस्ती स्वयंसेवक शिविर में बन्द कर रखा था, गाँधीजी के उस प्रस्ताव का अप्रिय रूप में विरोध करने वाले थे, जो उन्होंने इरविन को बधाई देने के लिए रखा था। इसी स्वयंसेवक शिविर में कदाचित् पहली बार कांग्रेस के मंच से ‘इन्कलाब जिंदाबाद’ का नारा लगाया गया था। 1929 में बी.एस-सी. करके अंग्रेजी एम.ए. में ये दाखि़ल हुए। इसी साल ये क्रांन्तिकारी दल में भी प्रविष्ट हुए।
इनके साथ थे देवराज, कमलकृष्ण और वेदप्रकाश नन्दा। कॉलेज में जिन दो अध्यापकों ने सबसे अधिक इन्हें प्रभावित किया, वे थे जे.एम. बनेड और डेनियल। जे.एम. बनेड ने तो इन के जेल जाने पर भी अपना स्नेह-सम्बन्ध बनाये रखा। बनेड ने ही (यद्यपि वे अध्यापक थे भौतिकशास्त्र के) विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की प्रेरणा दी। प्रो. डेनियल ने इन्हें ब्राउनिंग की ओर उन्मुख किया। इनके क्रान्तिकारी जीवन की अवधि 1921 से प्रारम्भ होकर 1936 तक है। इस अवधि का अधिकांशतः इतिहास देश के इतिहास से सम्बद्ध है। उसमें कहने की इतनी बातें हैं कि यहाँ उन पर विस्तार में विचार करना अनावश्क है। घटनाक्रम कुल यह है कि पहला कार्यक्रम इनका और इनके साथियों का भगतसिंह को छुड़ाने का हुआ। इस बीच में भगवतीचरण बोहरा एक दुर्घटना में शहीद हुए और यह कार्यक्रम स्थगित हो गया। दूसरा कार्यक्रम दिल्ली-हिमालयन टॉयलेट्स फैक्टरी के बहाने बम बनाने का कारखाना कायम करने का था। उस फैक्टरी में अज्ञेय वैज्ञानिक के रूप में सलाहकार थे। तीसरा कार्यक्रम अमृतसर में ऐसी फैक्टरी क़ायम करने का शुरू हुआ और यहीं देवराज और कमलकृष्ण के साथ 15 नवम्बर 1930 को गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तारी के बाद एक महीने लाहौर किले में, फिर अमृतसर की हवालात में। यहीं से यातना शुरू हुई। आर्म्स एक्ट वाले मुक़दमे में ये छूटे, पर फिर दिल्ली में 1931 में नया मुक़दमा शुरु किया गया। यह मुक़दमा 1933 तक चलता रहा। दिल्ली में ही काल कोठरी में बंद रहे और यद्यपि यहीं रहकर छायावाद से लेकर मनोविज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र और कानून-ये सारे विषय पढ़े। यहीं रह कर ‘चिन्ता’ और ‘शेखर’ लिखा, पर यह पूरी अवधि कुल ले-देकर घोर आत्ममन्थन, शारीरिक यातना और स्वप्न-भंग की पीड़ा की अवधि रही। 1934 की फरवरी में छूटे, फिर लाहौर में दूसरे कानून के अन्तर्गत नज़रबन्द किये गये। यहीं रह कर ‘कोठरी की बात’ और चिन्ता के कुछ अंशों की रचना की और इसी अवधि में कहानियों का छपना हुआ।
1986 में उनका अमृत महोत्सव मनाया गया-जो अमृत महोत्सव मनाया गया, वह बहुत ही सार्थक था। उसकी स्मृतियों में एक स्मृति मेरे मन पर गहरी छाप छोड़े हुए है। कुमार गंधर्व ने मीरां और कबीर के पदों का गायन किया था, उसमें एक पद के बोल थे ‘‘हम सब में, सब हम में, हम फिर बहुरि अकेला।’’ मुझे आज लगता है कि वह पद उनमें समा गया है, उनका वह भरा हुआ अकेलापन कहीं दूर ध्रुव तारे की तरह दिग्बोध कराता है और कहता है राह तुम्हारी हो, तुम्हारी बनायी हो, दिशाएँ बंधन नहीं है-दिशाएँ मुक्त हैं, ठहराव से। ऐसे व्यक्ति की जीवनी किस अनुक्रम में बाँधे समझ में नहीं आता। वहाँ से शुरू करें, जहाँ से मैं उन्हें जानता हूँ या वहाँ से शुरू करें, जिसके बारे में उनसे जाना है। बहुत कुछ उनकी भी स्मृति में नहीं है-मुझसे पन्द्रह वर्ष का यह अन्तर उन्होंने रखा ही नहीं और यह भ्रम ही पैदा किया कि हम आगे पीछे ही जन्मे हुए हैं। जब से उन्हें जाना, तब से उन्हें भाई ही कहा, भाई ही मानता रहा और वे भी भाई ही कहते रहे, केवल जब परिहास या उलाहने की मुद्रा में आते तो ‘पंडितजी’ कहते, ऐसे भाई की कहानी कहूँ या फिर अन्त से शुरू करें, जैसे कि महाभारत, श्रीमद्भागवत् जैसे काव्य-इतिहासों में हुआ है ? नहीं, मुझे जीवनी देनी है, एकदम सपाट नहीं, पर जीवनी क्रमबद्ध होती है, क्रमबद्ध ही जीवनी देने की कोशिश करूँगा।
उनका जन्म वत्स गोत्र के भणोत सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पितामह पंडित मूलचन्द शास्त्री ज्योतिषी थे-संस्कृत विद्या, कुलागत विद्या थी, उनका मूल अभिजन्म जालंधर जिले के कर्तापुर गाँव में। उनके पिता डॉ. हीरानन्द शास्त्री भारतीय पुरातत्व विभाग की सेवा में उच्च अधिकारी थे। वे संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित थे और प्राचीन लिपियों में ऐसे मर्मज्ञ थे, जैसे वे लिपियाँ उन्हें मिट्टी में मिली हों। उन्हें उन महत्त्वपूर्ण खुदाइयों का श्रेय प्राप्त है, जिन्होंने भारतीय इतिहास समझने के लिये सबसे स्पष्ट प्रमाण दिये हैं। कुशीनगर में भगवान् बुद्ध के महा-परिनिर्वाण स्थल को इन्होंने खोद निकाला है। नालन्दा की खुदाई ने भारतीय शिक्षा के केन्द्रों का आकार खड़ा किया। काशी में राजघाट की खुदाई ने कला-वैभव की रत्न-राशि दी। यद्यपि वे मोहन-जोदड़ों और हड़प्पा की संस्कृतियों के उद्घाटक थे, अंग्रेज साम्राज्य में यह श्रेय उनके अंग्रेज प्रभुओं को मिला। माँ दयावती देवी की चौथी संतान थे। सबसे सत्यवती जी, उनके बाद ब्रह्मानंद जी, उसके बाद जीवानन्द जी, जो 1934 में ही चल बसे; और उनसे छोटे वत्सराज जो बड़ौदा विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर वहीं रहते हैं। उसके बाद नित्यानन्द जी जो कि बिहार में क्रांतिकारी के रूप में कार्य करते रहे, वहीं बस गये हैं और उनसे छोटे पूर्णानंद जी जो काफ़ी कम उम्र में ही चले गये। उसके बाद रामानन्द जी और सबसे छोटी आनन्द लता जी, जिन्हें वे अन्ना जी कहकर बुलाते थे।
जन्म फल्गुन शुक्ल सप्तमी संवत् 1967 तदनुसार 7 मार्च, 1911 को कसया पुरतत्त्व-खुदाई शिविर में। बचपन 1911 से 15 तक लखनऊ में। शिक्षा का प्रारम्भ संस्कृत-मौखिक परम्परा से हुआ। 1915-19 तक श्रीनगर और जम्मू में। यहीं पर संस्कृत पंडित से रघुवंश, रामायण, हितोपदेश, फ़ारसी मौलवी से शेख़ सादी और अमेरिकी पादरी से अंग्रेज़ी की शिक्षा घर पर शुरू हुई। शास्त्रीजी को स्कूली शिक्षा में विश्वास नहीं था। बचपन में व्याकरण के पंडित से मेल नहीं हुआ। घर पर धार्मिक अनुष्ठान स्मार्त ढंग के होते थे। बड़ी बहन, जो लगभग आठ वर्ष बड़ी थी, जितना अधिक स्नेह करती थी, उतने ही दोनों बड़े भाई (ब्रह्मानन्द, जीवानन्द, जो 34 में दिवंगत हो गये) प्रतिस्पर्द्धा रखते थे। छोटे भाई वत्सराज के प्रति सच्चिदानन्द का स्नेह बचपन से ही था। 1919 में पिता के साथ नालन्दा आये, इसके बाद 1925 तक पिता के ही साथ रहे। पिताजी ने ही हिन्दी लिखाना शुरु किया। वे सहज और संस्कारी भाषा के पक्ष में थे। हिन्दुस्तानी के सख्त ख़िलाफ़ थे। नालन्दा से शास्त्रीजी पटना आये और वहीं स्व. काशीप्रसाद जायसवाल और स्व. राखालदास वन्द्योपाध्याय से इस परिवार का सम्बन्ध हुआ, पटना में ही अंग्रेज़ी से विद्रोह का बीज सच्चिदानंद के मन में अंकुरित हुआ। शास्त्रीजी के पुराने मित्र रायबदाहुर हीरालाल ही उनकी हिन्दी भाषा की लिखाई की जाँच करते। राखालदास के सम्पर्क में आने से बाड्ल़ा सीखी और इसी अवधि में इण्डियन प्रेस से छपी बाल रामायण, बाल महाभारत, बालभोज, इंदिरा (बंकिमचन्द्र) जैसी पुस्तकें पढ़ने को मिली और हरिनारायण आप्टे और राखालदास बन्द्योपाध्याय के ऐतिहासिक उपन्यास इसी अवधि में पढ़े गये। 1921-24 तक ऊटकमंड में रहे। यहाँ नीलगिरि की श्यामल उपत्यका ने बहुत अधिक प्रभाव डाला। 1921 में उडिपी के मध्वाचार्य के द्वारा इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसी मठ के पंडित ने छह महीने तक संस्कृत और तमिल की शिक्षा दी। इसी समय ‘भणोत’ से ‘वात्स्यायन’ में परिवर्तन भी हुआ, जो प्राचीनतम संस्कार को नये उत्साह से जीने का एक संकल्प था। पिता ने संकीर्ण प्रादेशिकता से ऊपर उठकर गोत्रनाम का प्रचलन कराया। इसी समय पहली बार गीता पढ़ी। पिताजी के आग्रह से अन्य धर्मों के ग्रन्थ भी पढ़े और घर पर ही पिताजी के पुस्तकालय का सदुपयोग शुरू किया। वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, लांगफेलो और व्हिटमैन की कविताएँ इस अवधि में पढ़ीं। शेक्सपियर, मारलो, वेब्स्टर के नाटक तथा लिटन, जार्ज एलियट, थैकरे, गोल्डस्मिथ, तोल्सतोय, तुर्गनेव, गोगोल, विक्टर ह्यूगो तथा मेलविल के उपन्यास भी पढ़े गये। लयबद्ध भाषा के कारण टेनिसन प्रभाव बड़ा गहरा पड़ा। टेनिसन के अनुकरण में, अंग्रेजी में ढेरों कविताएँ भी लिखीं।
उपन्यासकारों में ह्यूगों का प्रभाव, विशेष कर उनकी रचना ‘टॉयलर्स ऑफ दी सी’ का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इसी अवधि में विश्वेश्वर नाथ रेऊ तथा गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा की हिन्दी में लिखी इतिहास की रचनाएँ पढ़ने को मिलीं तथा मीरा, तुलसी के साहित्य का अध्ययन भी इन्होंने किया। साहित्यिक कृतित्व के नाम पर इस अवधि की देन है ‘आनन्द-बन्धु’ जो इस परिवार की निजी पत्रिका थी। इस पत्रिका के समीक्षक थे हीरालालजी और डाक्टर मोद्गिल। इसी अवधि में एक छोटा उपन्यास भी लिखा और इसी अवधि में जब मौट्रिक की तैयारी ये कर रहे थे, माँ के साथ इन्होंने जलियाँवाला बाग़ काण्ड की घटना के आसपास पंजाब की यात्रा की थी और अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह की भावना ने जन्म लिया था। एक घटना भी ब्लैकस्टोन नामक अंग्रेज़ अधिकारी के साथ घट चुकी थी। वह शास्त्रजी औऱ राखालदास के साथ यात्रा कर रहा था। डिब्बे में राखालदास की पत्नी भी थी। वह स्नानकक्ष से अर्द्धनग्न डिब्बे के भीतर आया। शास्त्रीजी ने उससे पूछा, ‘‘क्या इस रूप में तुम किसी अंग्रेज़ महिला के सामने आ सकते थे ?’’ उत्तर में वह कुछ बोला नहीं, हँसता रहा। शास्त्रीजी ने उसे ठठाकर डिब्बे से बाहर फेंक दिया। उसने आजीवन शत्रुता निभायी, यहाँ तक कि पिता द्वारा किये गये इस अपमान का बदला पुत्र से चुकाया, जब वे लाहौर क़िले में नज़रबन्द हुए।
दूसरी घटना का जिक्र वात्स्यायन ने संवत्सर में किया है। इनके पिताजी ने अपनी किसी पुरातत्व यात्रा में एक जगह देखी थी, जहाँ दो बूढ़े सिपाही तोप के गोले बनाते और किसी ढूह पर निशाना लगाते। एक तरह से उनके ऊपर इसका पागलपन छा गया था। ये दोनों बूढ़े सिपाही 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के बचे सिपाही थे। जो अंग्रेज़ों से प्रतिशोध लेने का यही उपाय निकाल सके थे और काल बीत गया था, परिस्थितियाँ बीत गयी थीं पर ये दोनों बूढ़े बीते काल के ऐसे संसक्त थे कि इनके लिये दूसरी वास्तविकता रह नहीं गयी थी। इस दृश्य का पंडित हीरानन्द शास्त्री पर गहरा प्रभाव पड़ा था और उस पागलपन में भी उन्हें एक दुर्धर्ष संकल्प दिखायी पड़ा था। शास्त्री जी सरकारी चाकरी में तो थे, पर अपने देश के लिये अभिमान और देश के लिए स्वाधीनता का स्वपन दोनों ही उनके कर्म और उनके हिन्दी लेखन में उद्भासित थे। उन्होंने एक तरह से ऐसे लोगों का एक समुदाय ही बनाया था, जो कला-चिन्तन और इतिहास-चिन्तन में स्वदेशी हों। इस समुदाय में थे स्वर्गीय राखालदास बन्द्योपाध्याय, जिन्हें लोग आर्डी बनर्जी के नाम से अधिक जानते हैं, स्वर्गीय विश्वेश्वरनाथ रेऊ, गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी। इन सबका गहरा प्रभाव भाई पर पड़ा और उनका स्वदेशीपन इस धूप-छाँह में परिपक्व हुआ। इनके पिताजी कठोर थे, बड़े व्यवस्था-प्रिय भी थे पर अपने लड़कों में भाई को कुछ अधिक मानते थे, शायद अपना विफल मनोरथ उनमें चरितार्थ होना देखना चाहते थे, इसीलिये मैंने धूप-छाँह की उपमा दी।
तीसरी घटना ऊटी में स्वयं सच्चिदानन्द के साथ घटी थी, जब वे दो-तीन महीने अंग्रेज़ों के साथ स्कूल में पढ़ने गये। वहाँ अंग्रेज़ी लड़कों की मरम्मत कर के स्कूल में इन्हें कार्ड मिला, जिसे फेंककर ये घर चले आये। 1925 में पंजाब से मैट्रिक की प्राइवेट परीक्षा दी और उसी वर्ष इण्टरमीडिएट साइंस पढ़ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। यहाँ उन्होंने गणित, भौतिकशास्त्र और संस्कृत विषय लिये थे। यहाँ इनके अंग्रेज़ी के प्रोफ़ेसर हेण्डरसन ने (जिन्हें त्रिशंकु समर्पित की गयी) साहित्य के अध्ययन की प्रेरणा दी। ये स्वयं भारत की भक्त थे। इन्हीं के साथ रवीन्द्रनाथ ने अध्ययन की स्थापना की और रस्किन के सौन्दर्यशास्त्र तथा आचारशास्त्र का अध्ययन किया। कला-क्षेत्रों के बीच में घूमते-घूमते स्थापत्य और शिल्प दोनों का राग-बोध परिपक्व होता गया। दक्षिण के मन्दिर और नीलगिरि के दृश्य ने उन के व्यक्तित्व में प्रकृति-प्रेम और कला-प्रेम को निखार दिया। मद्रास में सामाजिक विषमता की चेतना जगने लगी थी और मन में जाति के विरुद्ध विद्रोह इसी अवधि में उमड़ना शुरू हुआ। शास्त्रीजी स्वयं जाति में विश्वास न करके वर्ण में विश्वास करते थे और पुत्रों से आशा करते थे कि ब्राह्मण वर्ण का स्वभाव-त्याग, अभय और सत्य-उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
बचपन से किशोरावस्था तक की यह अवधि उलझन और आकुलता के बीच कठिन अध्यवसाय की अवधि है। एक ओर परिवार के और बाहर के अनेक प्रकार के प्रिय-अप्रिय प्रभावों ने उन के चित्त को उद्वेलित किया, तो दूसरी ओर पिता के कठिन अनुशासन ने परिश्रम में लगातार लगाये रखकर मन और शरीर को संयम में ढाला। बचपन में इन्हें ‘सच्चा’ के नाम से पुकारा जाता था और जब-जब इन की सच्चाई पर विश्वास नहीं किया गया, इन्होंने मौन विद्रोह किया।
बड़ी बहन जी ने बताया था कि एक बार पिताजी की कोई चीज़ मिल नहीं रही थी। भाई को मालूम था कि किसने ली थी। पिताजी ने एक-एक कर सबसे पूछे-तुमने ली है ? सबने पिटाई के डर से इन्कार कर दिया। भाई ने भी इन्कार किया और सबका क्रोध इन पर उतरा। पिटाई के बीच में भी चिल्लाते रहे कि मैं जानता हूँ किसने ली है, पर मैं बताऊँगा नहीं। बड़ी बहन रक्षा में खड़ी हो गयी-सच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, न कभी किसी की शिकायत करेगा। वे विनोद से कहती थी कि वह हमेशा से बड़ा ज़िद्दी रहा है, जो ठान ले, करके रहेगा।
एक बार की घटना ऐसी है कि बड़े भाई में और इसमें होड़ लगी कि चौदह रोटी कौन खा सकता है। बड़े भाई ने कहा कि तुम खोओ तो तुम्हें मैं इनाम दूँगा। ये खाने बैठे, पिताजी को इसकी सूचना मिली, उन्होंने बड़े भाई को डाँटा और इनसे कहा कि तुम अब न खाओ, उठ जाओ। ये चौदह के आसपास तक पहुँच रहे थे, अपने मन से उठे नहीं इसलिए इन्होंने भाई से इनाम माँगा। उन्होंने देने से इनकार कर दिया तो मौन विरोध में इसलिए खाना ही कम कर दिया। इस प्रकार की आत्म-पीड़क क्रोध इनमें बहुत दिनों तक रहा हौ और इसी क्रोध में आकर इन्होंने अपनी आर्थिक बर्बादी भी कम नहीं की है।
1927 में लाहौर के फोरमैन कॉलेज में ये बी.एस.सी में भर्ती हुए। इसी कॉलेज में नवजवान भारत सभा के सम्पर्क में आये और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख सदस्य आज़ाद, सुखदेव और भगवतीचरण बोहरा से परिचय हुआ। इस कॉलेज में बी.एस.सी. तक तो ये सक्रिय रूप से क्रान्तिकारी आन्दोलन में प्रविष्ट नहीं हुए थे, यद्यपि 1921 में पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ, उसमें ये स्वयंसेवक अफ़सर के रूप में मौजूद थे। यहीं इन्हीं के स्वयंसेवक दल ने उन लोगों को ज़बरदस्ती स्वयंसेवक शिविर में बन्द कर रखा था, गाँधीजी के उस प्रस्ताव का अप्रिय रूप में विरोध करने वाले थे, जो उन्होंने इरविन को बधाई देने के लिए रखा था। इसी स्वयंसेवक शिविर में कदाचित् पहली बार कांग्रेस के मंच से ‘इन्कलाब जिंदाबाद’ का नारा लगाया गया था। 1929 में बी.एस-सी. करके अंग्रेजी एम.ए. में ये दाखि़ल हुए। इसी साल ये क्रांन्तिकारी दल में भी प्रविष्ट हुए।
इनके साथ थे देवराज, कमलकृष्ण और वेदप्रकाश नन्दा। कॉलेज में जिन दो अध्यापकों ने सबसे अधिक इन्हें प्रभावित किया, वे थे जे.एम. बनेड और डेनियल। जे.एम. बनेड ने तो इन के जेल जाने पर भी अपना स्नेह-सम्बन्ध बनाये रखा। बनेड ने ही (यद्यपि वे अध्यापक थे भौतिकशास्त्र के) विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की प्रेरणा दी। प्रो. डेनियल ने इन्हें ब्राउनिंग की ओर उन्मुख किया। इनके क्रान्तिकारी जीवन की अवधि 1921 से प्रारम्भ होकर 1936 तक है। इस अवधि का अधिकांशतः इतिहास देश के इतिहास से सम्बद्ध है। उसमें कहने की इतनी बातें हैं कि यहाँ उन पर विस्तार में विचार करना अनावश्क है। घटनाक्रम कुल यह है कि पहला कार्यक्रम इनका और इनके साथियों का भगतसिंह को छुड़ाने का हुआ। इस बीच में भगवतीचरण बोहरा एक दुर्घटना में शहीद हुए और यह कार्यक्रम स्थगित हो गया। दूसरा कार्यक्रम दिल्ली-हिमालयन टॉयलेट्स फैक्टरी के बहाने बम बनाने का कारखाना कायम करने का था। उस फैक्टरी में अज्ञेय वैज्ञानिक के रूप में सलाहकार थे। तीसरा कार्यक्रम अमृतसर में ऐसी फैक्टरी क़ायम करने का शुरू हुआ और यहीं देवराज और कमलकृष्ण के साथ 15 नवम्बर 1930 को गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तारी के बाद एक महीने लाहौर किले में, फिर अमृतसर की हवालात में। यहीं से यातना शुरू हुई। आर्म्स एक्ट वाले मुक़दमे में ये छूटे, पर फिर दिल्ली में 1931 में नया मुक़दमा शुरु किया गया। यह मुक़दमा 1933 तक चलता रहा। दिल्ली में ही काल कोठरी में बंद रहे और यद्यपि यहीं रहकर छायावाद से लेकर मनोविज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र और कानून-ये सारे विषय पढ़े। यहीं रह कर ‘चिन्ता’ और ‘शेखर’ लिखा, पर यह पूरी अवधि कुल ले-देकर घोर आत्ममन्थन, शारीरिक यातना और स्वप्न-भंग की पीड़ा की अवधि रही। 1934 की फरवरी में छूटे, फिर लाहौर में दूसरे कानून के अन्तर्गत नज़रबन्द किये गये। यहीं रह कर ‘कोठरी की बात’ और चिन्ता के कुछ अंशों की रचना की और इसी अवधि में कहानियों का छपना हुआ।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i